नन्द दुलाल भट्टाचार्य, हक़ीकत न्यूज़, कोलकाता : ब्रेनवॉशिंग एक शब्द है जो प्रचार, उपदेश, अनुनय और जबरदस्ती जैसी विभिन्न मनोवैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से लोगों के विश्वासों, दृष्टिकोण और व्यवहार में हेरफेर को संदर्भित करता है या दूसरे शब्दों में कहें की एक धारणा ,विचार या मत को इस तरह से प्रस्तुत करना की लगे यही सबसे सर्वोत्तम है। ब्रेनवॉशिंग का उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए भी अक्सर किया जाता है, जैसे किसी निश्चित उम्मीदवार या पार्टी का समर्थन करने या अपने प्रतिद्वंद्वियों का विरोध करने के लिए मतदाताओं को प्रभावित करना। राजनीतिक क्षेत्र में ब्रेनवॉशिंग की प्रभावशीलता के कई पहलु हैं क्योंकि यह कई कारकों ( स्रोत, संदेश, श्रोता, संदर्भ ) पर निर्भर करता है। ब्रेनवॉशिंग एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण है और इसे इस्तेमाल करने वाला अगर शब्दों की कारीगरी ( Jugglery of words ) में माहिर हो तो किसी भी तरह के विचार, मत और व्यक्तित्व में बदलाव ला सकता है। ब्रेनवॉशिंग आपके मस्तिष्क के कामकाज के तरीके को बदलने के लिए तीव्र भावना के क्षणों का उपयोग करता है। इस विधि का उपयोग अच्छे के लिए भी किया जा सकता है और बुरे के लिए भी। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार यह दिमाग को पूरी तरह से हेरफेर या सोचने की प्रक्रिया को बदलने में बहुत हद तक कारगर साबित हुआ है। आज कल राजनितिक माहौल एक ध्रुवीकृत समय से गुजर रहा है । अगर हम समाचार पत्रिका या टेलीविज़न में प्रतिद्वंद्वी राजनितिक दलों और व्यक्तित्वों को देखें तो सकारात्मक और रचनात्मक आलोचना के बजाय सिर्फ नवीनतम झड़पें ही नज़र आयेंगी। राजनीति एक गंभीर और सकारात्मक विषय से ज्यादा खेल का मैदान महसूस होता है।
इतिहास
वर्तमान समाज में ब्रेनवॉशिंग (विचार नियंत्रण) की भूमिका को समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास के पन्नों को उलटने की जरूरत है की इस प्रक्रिया की शुरुआत कैसे और किस सन्दर्भ में हुई और इस ब्रेनवॉशिंग के पीछे का मनोविज्ञान क्या है। ब्रेनवॉशिंग (विचार नियंत्रण) एक दिलचस्प और जटिल विषय है जिसने बीसवीं और इक्कीसवीं सदी के इतिहास और राजनीति को बहुत हद तक प्रभावित किया था। यह मानव मनोविज्ञान की प्रकृति, विचारधारा की शक्ति और स्वतंत्रता और स्वायत्तता की सीमाओं के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। १९५० (1950) में, एक अमेरिकी पत्रकार ने ‘ब्रेनवॉशिंग’ शब्द को यह तर्क देते हुए लोकप्रिय बनाया कि प्रौद्योगिकी ( technology ) और विचारधारा (ideology ) का एक नया मिश्रण लोगों के सोचने, समझने की प्रक्रिया पर बहुत गहरा प्रभाव डाल रहा है । ‘ब्रेनवॉश्ड- ए -न्यू- हिस्ट्री ऑफ थॉट कंट्रोल'(‘Brainwashed, A New History of Thought Control’) के इस संक्षिप्त लेख में मनोविश्लेषक और इतिहासकार डैनियल पिक यह बताते हैं कि हम जो सोचते समझते हैं उसे कैसे प्रभावित किया जा सकता है।
हमारे देश के राजनितिक माहौल के सन्दर्भ में ब्रेनवॉशिंग (विचार नियंत्रण) की परिभाषा
हमारे देश के मौजूदा राजनितिक माहौल में यह ब्रेनवॉशिंग या विचार/ सोच नियंत्रण की प्रक्रिया में कौन से करक शामिल है इस पर थोड़ा नज़र डालते हैं। हमारे देश में किसी विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में मतदाताओं को प्रभावित करने में मीडिया की भूमिका एक जटिल और विवादास्पद विषय है। मीडिया जनता को सूचित करने, शिक्षित करने और संगठित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। भारतीय मीडिया परिदृश्य की विविधता जिसमें पारंपरिक मीडिया (जैसे समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविजन), सोशल मीडिया (जैसे फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप),और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म (जैसे समाचार वेबसाइट, ब्लॉग और पॉडकास्ट ) शामिल हैं। लेकिन इसका उपयोग मतदाताओं की सोच नियंत्रण और ध्रुवीकरण करने के लिए भी शायद किया जा रहा है। हमारे देश की चुनावी प्रक्रियायों में मीडिया की भूमिका को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। मीडिया आउटलेट्स का स्वामित्व और विनियमन, जो मालिकों, विज्ञापनदाताओं या सरकार के राजनीतिक और आर्थिक हितों को प्रतिबिंबित कर सकता है। कुछ मीडिया आउटलेट कुछ राजनीतिक दलों या विचारधाराओं से संबद्ध या वित्त पोषित हो सकते हैं, जबकि अन्य स्वतंत्र या तटस्थ हो सकते हैं। मीडिया उपभोक्ताओं की पहुंच और साक्षरता, जो मतदाताओं के क्षेत्र, भाषा, जाति, वर्ग, लिंग और उम्र के आधार पर भिन्न हो सकती है। कुछ मतदाता जानकारी के एक ही स्रोत पर भरोसा कर सकते हैं, जबकि अन्य जानकारी की जांच और सत्यापन करने के लिए कई स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं। मीडिया कवरेज की सामग्री और गुणवत्ता, जो प्रदान की गई जानकारी की सटीकता, संतुलन, प्रासंगिकता और गहराई के संदर्भ में भिन्न हो सकती है। कुछ मीडिया आउटलेट तथ्यात्मक और वस्तुनिष्ठ रिपोर्टिंग प्रस्तुत कर सकते हैं, जबकि अन्य मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए सनसनीखेज, प्रचार या नकली समाचार का उपयोग कर सकते हैं। कुछ अध्ययनों के अनुसार, मीडिया भारतीय मतदाताओं के मतदान व्यवहार और प्राथमिकताओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने में बहुत हद तक सक्षम है, खासकर सोशल मीडिया के संदर्भ में, जो हाल के वर्षों में राजनीतिक संचार और प्रचार का एक प्रमुख माध्यम बन गया है। सोशल मीडिया राजनीतिक अभिनेताओं और मतदाताओं के बीच प्रत्यक्ष और संवादात्मक जुड़ाव को सक्षम कर सकता है, साथ ही समर्थकों के बीच समुदाय और पहचान की भावना पैदा कर सकता है। हालाँकि, सोशल मीडिया लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए चुनौतियाँ और जोखिम भी पैदा कर सकता है, जैसे गलत सूचना फैलाना, घृणास्पद भाषण, हिंसा इत्यादि । इसलिए, भारतीय चुनावों में मीडिया की भूमिका सरल या सीधी नहीं है, बल्कि गतिशील है। मीडिया अच्छे या बुरे के लिए एक ताकत हो सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि राजनीतिक दलों और मतदाताओं द्वारा इसका उपयोग और उपभोग कैसे किया जाता है। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, हमारे सामने आने वाले मीडिया स्रोतों और संदेशों के प्रति जागरूक और आलोचनात्मक होना और अपने स्वयं के सूचित और स्वतंत्र निर्णय के आधार पर वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करना बहुत ही महत्वपूर्ण है।
उपसंहार
प्रजातंत्र में आम इंसान को सर्वोपरि रखा गया है। दूसरे शब्दों में आम इंसान को भाग्यविधाता भी कहा जाता है जो अपने वोट अधिकार के माध्यम से आम को खास और खास को आम बनाने की ताकत रखते हैं। इसीलिए चुनावी नतीजों को जनादेश कहा जाता है जिसमे जन यानी आम इंसान निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को आदेश देता है की वह उनका प्रतिनिधित्व करते हुये देश की बागडोर संभालकर जन के हित में काम करे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है की चुनाव में जितने के बाद ये जनप्रतिनिधि सिर्फ सत्ता के क्रमपरिवर्तन और संयोजन में लिप्त हो जाते हैं। इस प्रजातंत्र के महापर्व यानी निर्वाचन प्रक्रिया में कौन कितना बड़ा नेता या तथाकथित बुद्धिजीवी या विश्लेषक है या जानकारी कितने बड़े मीडिया हाउस से आ रही है इससे भी महत्वपूर्ण है जमीनी सच्चाई को पहचानना। दुर्भाग्य की बात है इन ७५ ( 75) सालों में कितने चुनाव आये और गये राजनीतिक सत्ता भी कई हाथों में बदली है पर बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाएं , सामाजिक सुरक्षा, सिर पर एक छत, कुपोषण, जैसे बुनियादी मुद्दों पर आज भी आम इंसान को जद्दो-जहद्द करना पर रहा है। यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि कुछ सतही और कॉस्मेटिक समाधान के अलावा किसी भी राजनेता या राजनीतिक दल ने निष्पक्ष, समयबद्ध और परिणामोन्मुख तरीके से इन मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया है। समय आ गया है कि नीति निर्माताओं को अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करने की जरूरत है, देश को अर्थव्यवस्था में रोजगारविहीन विकास की जरूरत से ज्यादा पर्याप्त रोजगार सृजन के साथ आर्थिक विकास की जरूरत है। धन का असमान वितरण और बेरोज़गारी वृद्धि लंबे समय तक आर्थिक विकास को कायम नहीं रख सकती है। नीति निर्माताओं और नीति कार्यान्वयनकर्ताओं दोनों को जमीनी हकीकत को समझते हुए अपने सहज क्षेत्र ( comfort zone) से बाहर आने की जरूरत है। सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में वृद्धि किसी देश के स्वास्थ्य को मापने का एकमात्र पैमाना नहीं हो सकता है ।
बिधिवत सतर्कीकरण एवं डिस्क्लेमर (अस्वीकरण) : इस समाचार में दिया गया वक़्तवय और टिप्पणी एक निरपेक्ष न्यूज़ पोर्टल की हैसियत से उपलब्ध तथ्यों और समीक्षा के आधार पर दिया गया है। हमारा उदेश्य किसी संगठन/ प्रतिष्ठान/ राजनितिक दल की कार्यशैली पर इच्छानुरूप टिप्पणी या किसी व्यक्ति या समूह पर अपने विचार थोपना नहीं है । (हकीक़त न्यूज़ www.haqiquatnews.com) अपने सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति पूरी तरह से जागरूक न्यूज़ पोर्टल है।
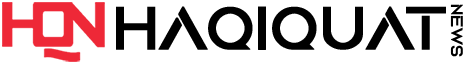

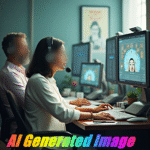





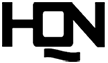









Add Comment