नन्द दुलाल भट्टाचार्य, हक़ीकत न्यूज़, कोलकाता : हमारे देश की शिक्षा प्रणाली ने अपनी स्थापना के बाद से अब तक काफी कुछ बदलाव देखे हैं। बदलते समय और समाज में बदलाव के साथ के साथ हमारी शिक्षा प्रणाली में भी कुछ बदलाव आया है हालांकि, ये बदलाव और विकास अच्छे के लिए हैं या नहीं यह अभी भी एक बड़ा सवाल है? ऐसे समय में, जब विश्व रचनात्मक और उत्साही व्यक्तियों की तलाश में हैं, भारतीय स्कूल युवा मन को किताबी ज्ञान से प्रशिक्षित कर रहे हैं जो उन्हें रचनात्मक व्यक्ति बनने के बजाय बस किताबी कीड़ा बना रहा है । सुझाव देने या विचारों को साझा करने की कोई स्वतंत्रता नहीं है। भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार की गंभीर आवश्यकता है । वैश्वीकरण को ध्यान में रखते हुए और समय के मांग के अनुसार यदि हम नवीन शोध करना चाहते हैं तो शिक्षा प्रणाली में अभिनव ,रचनात्मक और सकारात्मक बदलाव लाने की सख्त जरूरत है। हालाँकि, दुर्भाग्य से हमारे स्कूल हमें इस तरह से प्रशिक्षित नहीं करते हैं। अगर हम अपने शिक्षा प्रणाली को जरह सूक्ष्म तरीके से देखें तो हमें एक निर्धारित अध्ययन प्रणाली नज़र आयेगी और सिर्फ सैद्धांतिक सबक सीखने की तरफ ही जोर दिया जाता हैं, रचनात्मकता के लिए कोई जगह नहीं बची है। रचनात्मक सोच के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली को बदलने की बहुत जरूरत है । स्कूलों को उन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो छात्र के दिमाग को चुनौती देते हैं, उनके विश्लेषणात्मक कौशल को सुधारते हैं और उनकी रचनात्मक सोच क्षमता को बढ़ाते हैं। इससे उन्हें अलग-अलग क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी। हमारी यह रटने वाली शिक्षा प्रणाली के मूल कारण को समझने के लिए थोड़ा इतिहास के पन्नों को उलटना पड़ेगा। जब ब्रिटिश हुक़ूमत हमारे देश में राज कर रहे थे तो उनके सामने दो बड़ी चुनौतियाँ थीं एक भारतीयों के साथ वार्तालाप (communication) और दूसरा कर्मियों और क्लर्क की उन्हें बहुत जरूरत थी और तब थॉमस बबिंगटन मैकाले (Thomas Babington Macaulay ) द्वारा अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम १९३५ (1835) दिया गया जिससे उनके दोनों उद्देश्य पुरे हो गये पहला उनको आदमी चाहिए थे जो चुप चाप डेस्क पे बैठें और अपना काम करें और ज्यादा प्रश्न न करें और रचनात्मक ( creative) तो बिलकुल न हों और दूसरा अंग्रेजी भाषा में वार्तालाप। और यहीं से शुरू हुई रटने वाली शिक्षा पद्धति जो आज तक चली आ रही है। अगर हम अपनी शिक्षा प्रणाली को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो साफ फर्क नज़र आयेगा। जितनी स्विजरलैंड की कुल जनसंख्या है उससे ज्यादा तो हमारे देश ने इंजीनियर पैदा कर दिए हैं। उसके बाद भी रिसर्च एंड इनोवेशन पे स्विजरलैंड नंबर एक पर है। स्वाधीनता के बाद से हमारे देश ने साइंस में शून्य नोबल लॉरिएट पैदा किये हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका ने सौ पार कर दिये हैं। ASER के रिपोर्ट के अनुसार ८३ (83) प्रतिशत शिक्षित भारतीय रोजगार योग्य नहीं हैं। और यह जो सुंदर पिच्चई और सत्य नडेला की हम बात करतें हैं इन्होंने भी अपनी उच्चतर शिक्षा विदेशों से प्राप्त की है। अंग्रेजी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा नहीं है इसके बावजूद भी अंग्रेजी एक भाषा की जगह एक क्लास बन गया है भारत में। रूस, चाइना, फ्रांस, जापान जैसे देशों में अंग्रेजी भाषा को लेकर इतना जुनून नहीं है जितना हमारे देश में है। पुअर कम्युनिकेशन बोला जाता है अगर आपकी अंग्रेजी बोलने की छमता अच्छी नहीं है तो। हमारे देश की शिक्षा प्रणाली में रटने की प्रतियोगिता होती है जो जितना ज्यादा रट लेता है तो उसके उतने अच्छे अंक आते हैं।भारतीय शिक्षा प्रणाली दुनिया भर में सबसे पुरानी शिक्षा प्रणालियों में से एक होने के बावजूद यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बदलते समय और तकनीकी प्रगति के साथ अन्य राष्ट्रों की शिक्षा प्रणालियों में बड़े बदलाव आए हैं, लेकिन हम अभी भी पुरानी और सांसारिक प्रणाली के साथ फंसे हुए हैं। शिक्षा की पूरी प्रणाली जिसमे, छात्र, शिक्षक, स्कूल, अभिवावक सभी शामिल हैं और इसी सोच के साथ भाग रहें हैं की छात्र परीक्षा में दिये गये प्रश्नों में किसी भी तरह ८० (80) से ९० (90) प्रतिशत प्रश्न सही -सही हल कर लें। पूरा रास्ता ही ऐसा बन गया है शिक्षक को जल्दी -से -जल्दी और ज्यादा-से-ज्यादा पाठ्यक्रम कवर करते हुये पढ़ाना है। प्रयोग आधारित प्रश्न तो हैं पर सही मायने में प्रयोग गायब हैं। कक्षा में समझना और रटना बहुत ज्यादा शिक्षक के पढ़ाने की पध्दति पर भी निर्भर करता है। न तो हमारी प्रणाली ने पाठ्यक्रम में कोई बड़ा बदलाव देखा है और न ही शिक्षा प्रदान करने के तरीके में कोई महत्वपूर्ण बदलाव आया है।समझने , याद करने और रटने में बहुत अंतर है अगर हम शिक्षण पध्दति की तरफ ज़रा ध्यान से देखें तो सिखाने की प्रक्रिया भी समझने से ज्यादा रटने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करती है। ज्यादातर प्रश्न और उनके उत्तर लिखवा दिए जातें हैं और उनको समझने के बजाय बस रट लें इससे निचली कक्षाओं में तो छात्र निकल जाते हैं पर उच्च कक्षाओं में समस्याएं शुरू होती हैं जहाँ एक छात्र अपने आपको समझने की प्रक्रिया में खुद को ढालने में असमर्थ महसूस करता है। स्कूल ड्रॉपआउट के कारक तो बहुत सारे हैं पर यह रटने की प्रक्रिया से उभरकर समझने की प्रक्रिया में खुद तो ढालने की असमर्थता भी एक कारण है इसीलिए अगर स्कूल ड्रॉपआउट की तरफ नज़र डालें तो ज्यादातर ड्रॉपआउट उच्च कक्षाओं में पाये जायेंगे। शायद वक़्त आ गया है की हुक्मरानों को समझने की आवश्यकता है की हमारे देश की शिक्षा प्रणाली में गंभीर सुधारों की आवश्यकता है। रटने वाली शिक्षा प्रणाली से बाहर निकलकर अभिनव, रचनात्मक प्रणाली की ओर बढ़ने की सख्त जरूरत है। प्रौद्योगिकी बहुत तेज गति से बदल रही है और शिक्षण तकनीकों को वर्तमान तकनीक के साथ तेजी से बदलने की आवश्यकता है अन्यथा आने वाले कल में हमारे देश को बड़ी संख्या में शिक्षित बेरोजगारों की कठोर वास्तविकता का सामना करना पड़ेगा।
बिधिवत सतर्कीकरण एवं डिस्क्लेमर (अस्वीकरण) : इस समाचार में दिया गया वक़्तवय और टिप्पणी एक निरपेक्ष न्यूज़ पोर्टल की हैसियत से उपलब्ध तथ्यों और समीक्षा के आधार पर दिया गया है। हमारा उदेश्य किसी भी संगठन/ प्रतिष्ठान/ या राजनितिक दल की कार्यशैली पर इच्छानुरूप टिप्पणी या किसी व्यक्ति या समूह पर अपने विचार थोपना नहीं है। हम ऊँगली नहीं सही मुद्दे उठाते हैं। समस्यायों को सही कानो तक पहुँचाना और सवालों को सही हल तक ले जाना ही हमारा मकसद है। (हकीक़त न्यूज़ www.haqiquatnews.com) अपने सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति पूरी तरह से जागरूक न्यूज़ पोर्टल है।
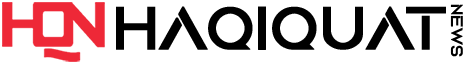

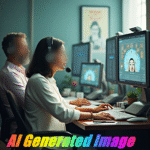





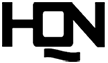









Add Comment